कमजोर
होती कांग्रेस के कारण यू.पी.ए में बेचैनी और क्षेत्रीय क्षत्रपों की बढ़ती
महत्वाकांक्षाएं
२०१४ के आम चुनावों से पहले पांच
राज्यों के विधानसभा चुनावों को ‘सत्ता का सेमीफाइनल’ माना जा रहा था. आश्चर्य
नहीं कि इन चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी थी. खासकर
उत्तर प्रदेश इस राजनीतिक जंग का मैदान बन गया था.
लेकिन मजा देखिए कि इन चुनावों
खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के कारण
मध्यावधि चुनावों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. माना जा रहा है कि इन चुनावों में
कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति के कारण न सिर्फ यू.पी.ए के घटक दलों में बेचैनी है
बल्कि कांग्रेस विरोधी दलों में मौके का फायदा उठाने की जल्दी भी दिखाई देने लगी
है.
हैरानी की बात नहीं है कि राष्ट्रीय और
क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के बीच नए तालमेल और गठबंधनों की सुगबुगाहट जोर
पकड़ने लगी है. यू.पी.ए के अंदर और बाहर तृणमूल कांग्रेस (ममता बैनर्जी), जयललिता
(अन्नाद्रमुक), मुलायम सिंह यादव (सपा), नवीन पटनायक (बी.जे.डी) और नीतिश कुमार (जे.डी-यू)
जैसे क्षेत्रीय नेता और पार्टियां इस मौके का फायदा उठाने के लिए जल्दी चुनाव
चाहती हैं.
हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद भी कमजोर स्थिति में है और इन चुनावों
और खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी पतली हालत के मद्देनजर वह भी तुरंत चुनाव को लेकर
बहुत उत्साहित नहीं है.
लेकिन इस साल के आखिर में गुजरात और
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन के मुताबिक भाजपा भी चुनाव के
लिए तत्पर हो सकती है. निश्चित ही, भाजपा कुछ महीने और इंतज़ार करना चाहती है लेकिन
एन.डी.ए के घटक दलों जैसे अकाली दल, जे.डी.-यू और शिव सेना के दबाव में वह जल्दी
चुनाव के लिए भी तैयार हो सकती है.
भाजपा इसलिए भी चुनाव के पक्ष में तैयार हो
सकती है कि वह गैर कांग्रेस-गैर भाजपा तीसरे या चौथे मोर्चे के गठन को रोकना
चाहेगी. साथ ही, उसे यह भी लग रहा है कि राज्य विधानसभा चुनावों के विपरीत
राष्ट्रीय चुनावों में कांग्रेस विरोधी माहौल का सबसे अधिक फायदा उसे ही मिल सकता
है.
हालांकि कांग्रेस और दूसरी कई पार्टियां
तुरंत चुनाव टालना चाहती है और ताजा विधानसभा चुनावों के झटके से उबरने के लिए समय
चाहती है लेकिन यह भी सच है कि यू.पी.ए सरकार के लिए आने वाले महीने राजनीतिक रूप
से बहुत मुश्किल होनेवाले हैं.
विधानसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस की हार हुई
है और नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के खिलाफ लोक लुभावना राजनीति को समर्थन मिला
है, उसके कारण यह तय माना जा रहा है कि यू.पी.ए सरकार के लिए अब इन विवादस्पद
आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होगा.
जाहिर है कि जब मध्यावधि चुनाव नजदीक
दिख रहे हों तो कोई भी पार्टी यहाँ तक कि यू.पी.ए के घटक दल भी इन नव उदारवादी
आर्थिक सुधारों की कड़वी गोली खासकर खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई जैसे फैसलों को
निगलने के लिए तैयार नहीं होंगे.
यहाँ तक कि मनमोहन सिंह सरकार सब्सिडी में कटौती
खासकर खाद और पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोत्तरी जैसे फैसले भी करने की स्थिति में
नहीं रह गई है. साफ़ है कि व्यावहारिक रूप से यू.पी.ए सरकार एक कामचलाऊ सरकार में
बदल गई है जिसका राजनीतिक इकबाल काफी कमजोर हो गया है.
कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसी सरकार
जितने दिन सत्ता में रहेगी, उसकी उतनी ही दुर्गति होगी. खासकर उस कांग्रेस के लिए
यह किसी दु:स्वप्न से कम नहीं होगा जो २००९ के आम चुनावों में पुनर्वापसी और अपनी
राजनीतिक ताकत में बढ़ोत्तरी के बाद २०१४ के आम चुनावों में अकेले दम पर सत्ता में
लौटने का सपना देखने लगी थी.
लेकिन उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और गोवा में करारी हार
और कुछ हद तक उत्तराखंड में झटके के बाद उसे न सिर्फ घटक दलों के खींचतान और
मोलतोल के आगे झुकना पड़ेगा बल्कि सत्ता की मलाई में उन्हें कहीं बड़ी हिस्सेदारी
देनी पड़ेगी.
यही नहीं, खुद कांग्रेस में आंतरिक
असंतोष और गुटबंदी को हवा मिलेगी. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के युवराज राहुल
गाँधी के कथित जादू के न चलने से २०१४ के चुनावों में उसके सबसे बड़े ट्रंप कार्ड
की कलई खुल गई है. इससे कांग्रेस में मौके का इंतज़ार कर रहे उन गुटों को सिर उठाने
और हमला करने का मौका मिलेगा जो पार्टी में राहुल गाँधी और खासकर उनकी टीम के उभार
से असहज और नाराज हैं.
जाहिर है कि इससे पार्टी के अंदर और बाहर उसके नेताओं और
गुटों के बीच घात-प्रतिघात का खेल भी तेज हो जाएगा जो कांग्रेस आलाकमान की निर्णय
क्षमता को भी प्रभावित करेगा.
यह किसी से छुपा नहीं है कि पिछले कुछ महीनों
में जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रणब मुखर्जी, पी. चिदंबरम और
दूसरे बड़े नेताओं के बीच खींचतान और विवाद बढ़े हैं, उसके कारण सरकार की न सिर्फ
काफी किरकिरी हुई है बल्कि कई मामलों में सरकार नीतिगत और राजनीतिक तौर पर
लकवाग्रस्त भी हो गई है.
आश्चर्य नहीं होगा अगर आनेवाले महीनों में कांग्रेस
नेतृत्व के खिलाफ कुछ और बागी सुर भी सुनाई दें खासकर उन राज्यों में जहां
कांग्रेस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेसी नेताओं में
डूबते जहाज से भागने और पाला बदलने की खबरें भी जल्दी आने लगेंगी.
ऐसे में, कांग्रेस को यह भी सोचना पड़ेगा
कि वह अगला आम चुनाव राहुल गाँधी के नेतृत्व में लड़ने का जोखिम उठाए या नहीं?
हालांकि उसके पास गाँधी परिवार का कोई विकल्प नहीं है लेकिन उसे अपनी रणनीति पर
दोबारा विचार करना पड़ेगा कि राहुल गाँधी को अब कैसे और किस रूप में पेश किया जाए?
इससे पहले उसे इस साल के मध्य में होनेवाले राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनावों
में अपने प्रत्याशियों को जीताने के लिए खासा द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ेगा. राजनीतिक
रूप से महत्वपूर्ण इन दोनों चुनावों के लिए उसे न सिर्फ यू.पी.ए के घटक दलों को
संभालना पड़ेगा बल्कि विपक्ष खासकर गैर भाजपा दलों को साधना पड़ेगा.
यह इतना आसान नहीं होगा. बहुत संभव है
कि गैर भाजपा दल, एन.डी.ए के साथ अंदरखाते की सहमति से कोई ऐसा उम्मीदवार पेश कर
दें जिसके कारण यू.पी.ए में भी फूट पड़ जाए. इससे यू.पी.ए का राजनीतिक संकट बढ़ सकता
है और मध्यावधि चुनाव को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा.
जाहिर है कि कांग्रेस ऐसी
स्थिति आने से रोकने की कोशिश करेगी. इसके लिए उसे घटक दलों के अलावा अन्य प्रमुख
दलों के साथ मोलतोल में जाना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में, उसके लिए किसी कट्टर और गाँधी
परिवार के प्रति निष्ठावान कांग्रेसी को राष्ट्रपति बनाने का मोह छोड़ना पड़ेगा.
क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी?
दूसरे, वह खुद भी लंबे समय तक मौजूदा राजनीतिक गतिरोध और कामचलाऊ सरकार की
थुक्का-फजीहत से बाहर निकलना चाहेगी. यही नहीं, राजनीतिक अनिश्चितता और सरकार की
लकवाग्रस्त होती स्थिति से देशी-विदेशी बड़ी पूंजी और बड़े कारपोरेट समूहों में भी
भारी बेचैनी है जो इन चुनावों के बाद आर्थिक सुधारों के मामले में बड़ी घोषणाओं और
फैसलों का इंतज़ार कर रहे थे.
जाहिर है कि वे भी मौजूदा स्थिति को लंबे समय तक
बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे. आखिर बड़ी देशी-विदेशी पूंजी का सबसे अधिक
दांव पर लगा हुआ है. ऐसे में, बड़ी पूंजी और कारपोरेट समूहों
के दबाव में या तो कांग्रेस और भाजपा के बीच कुछ समय के लिए एक आंतरिक सहमति के
आधार नव उदारवादी आर्थिक सुधारों से संबंधित कम विवादास्पद विधेयकों को संसद में
पारित कराने और फिर अनुकूल समय पर चुनाव कराने की कामचलाऊ व्यवस्था बनेगी.
या फिर राजनीतिक
गतिरोध को तोड़ने के लिए इस साल के आखिरी महीनों में चुनाव का दबाव बनेगा. वैसे बड़ी
देशी-विदेशी पूंजी और उनके कारपोरेट प्रतिनिधि तुरंत चुनाव नहीं चाहते हैं.
इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आज की
राजनीतिक-सामाजिक स्थिति में बड़ी देशी-विदेशी पूंजी की दोनों प्रमुख प्रतिनिधि
पार्टियों- कांग्रेस और भाजपा को अकेले या उनके नेतृत्व वाले दोनों प्रमुख
गठबंधनों- यू.पी.ए और एन.डी.ए अकेले दम पर बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है.
इसका
अर्थ यह हुआ कि तत्काल चुनावों से राजनीतिक अस्थिरता और गतिरोध और अधिक बढ़ने की
आशंका है. यही नहीं, तीसरे मोर्चे जैसे प्रयोगों के साथ जुड़ी अनिश्चितता और
अस्थिरता के अलावा आर्थिक सुधारों के ठप्प पड़ने की आशंका के कारण बड़ी पूंजी और
कारपोरेट समूह ऐसी किसी स्थिति को टालने की हरसंभव कोशिश करेंगे.
लेकिन बड़ी पूंजी आम चुनावों को फिलहाल के
लिए टालने की कोशिशों में किस हद तक कामयाब होगी, यह कह पाना मुश्किल है लेकिन
इतना तय दिख रहा है कि वह कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति के मद्देनजर अपने नए
मोहरों को आगे बढ़ाने और जहां तक संभव हो, विकल्प के बतौर एन.डी.ए को मजबूत और आगे
करने की जुगत जुट गई है.
आश्चर्य नहीं होगी कि बड़े कारपोरेट समूह अगले कुछ महीनों
में भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी और एन.डी.ए की ओर से नीतिश कुमार के नामों को
आगे बढ़ाएं और चुनाव नतीजों के बाद नए राजनीतिक समीकरणों और सुभीते के लिहाज से इन
दोनों में से किसी को अगले नेता और सरकार गठन के लिए प्रस्तावित किया जाए.
लेकिन इन राजनीतिक हलचलों और मेलजोल के
बीच इस बार वामपंथी मोर्चा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक
रूप से हाशिए पर चला गया है. तीसरे मोर्चे की राजनीति करनेवाले क्षेत्रीय क्षत्रप
इस बार उसे कोई खास भाव नहीं दे रहे हैं. वह खुद भी अपनी कमजोर स्थिति के कारण
इसमें खास दिलचस्पी नहीं ले रहा है.
साफ़ है कि २००९ के आम चुनावों और उसके बाद
पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों में हार से उबर नहीं पाया है और तुरंत
चुनावों के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में हैरानी नहीं होगी कि वाम मोर्चा अंदरखाते
कांग्रेस के साथ एक समझ बनाकर परोक्ष रूप से यू.पी.ए की मदद करे.
असल में, माकपा दम साधे पश्चिम बंगाल
में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के नतीजे का इंतज़ार कर रही
है. उसकी सारी उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि किसी तरह कांग्रेस और तृणमूल का
गठबंधन टूटे और उसके बाद होनेवाले चुनावों में वह उन दोनों के बीच वोटों के
बंटवारे का लाभ उठा सके. लेकिन यह इतना आसान नहीं है.
इसके उलट यह संभव है कि
पश्चिम बंगाल में तृणमूल से अलग होने की स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल साफ़ हो जाए
और आमने-सामने के मुकाबले में तृणमूल, माकपा पर भारी पड़ जाए. ममता इसी कारण जल्दी
में हैं क्योंकि जितनी देर होगी, वायदों को पूरा न कर पाने के कारण उनकी सरकार के
खिलाफ राजनीतिक विरोध मजबूत होगा.
साफ़ है कि माकपा और उसके साथ वाम मोर्चा
इंतज़ार और दूसरी ओर, तृणमूल के बरक्स कांग्रेस के साथ साठगांठ की रणनीति पर चल रहा
है. माकपा इससे आगे नहीं सोच पा रही है और न ही किसी बड़े प्रयोग के लिए तैयार दिख
रही है.
हालांकि यह मौका है जब कांग्रेस भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, नई आर्थिक
नीतियों को आँख मूंदकर लागू करने और जल-जंगल-जमीन को देशी-विदेशी कारपोरेट को
हवाले करने से भड़के जन आन्दोलनों के कारण कमजोर हो रही है और दूसरी ओर, अपने
सांप्रदायिक और नई आर्थिक समर्थक रवैये के साथ-साथ अपनी राज्य सरकारों पर
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी भाजपा चढ़ नहीं पा रही है.
इससे देश में गैर कांग्रेस-गैर भाजपा एक
तीसरे मोर्चे की जरूरत और जगह बनी हुई है. लेकिन यह भी सच है कि बिना किसी वैचारिक
एकता, कार्यक्रम और राजनीतिक दिशा के बननेवाले ऐसे मोर्चे की सफलता इसलिए संदिग्ध
है क्योंकि जनता में उसकी विश्वसनीयता और साख नहीं बन पाती है. २००९ के चुनाव में
ऐसे प्रयोग का हश्र सब देख चुके हैं.
जाहिर है कि अगर इस नए तीसरे मोर्चे में भी
जयललिता, ममता, मुलायम, चन्द्रबाबू और नवीन पटनायक जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप होंगे
तो उसकी साख संदिग्ध ही रहेगी. इसके बजाय वामपंथी पार्टियों के लिए यह
समय वाम की स्वतंत्र दावेदारी का होना चाहिए.
उनके पास यह मौका है जब वे कांग्रेस
और भाजपा दोनों की कमजोर हालात के मद्देनजर आम लोगों के सवालों खासकर महंगाई,
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर देशव्यापी जनसंघर्षों
से अपनी स्वतंत्र दावेदारी पेश करने की कोशिश करें.
पिछली २८ फरवरी को नई आर्थिक
नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल ने इसकी जमीन तैयार कर दी है. वाम मोर्चे को इसे
आगे बढ़ाने और इसमें मोर्चे से बाहर की वाम, जनतांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियों को
एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए.
क्या वामपंथी पार्टियां इसके लिए तैयार हैं? या, वे फिर
उन्हीं राजनीतिक दलों के भरोसे जोड़तोड़ से तीसरा या चौथा मोर्चा बनाकर चुनावों में
उतरने की भूल करेंगी? मजबूरी में ही सही उनके सामने एक मौका है. क्या वे इस मौके
को गँवा देंगी?
दूसरी ओर, यह देश भर में नई आर्थिक नीतियों और साम्प्रदायिक
फासीवाद के खिलाफ गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और नौजवानों की लड़ाई
लड़ रही वाम और जनतांत्रिक शक्तियों के लिए भी एकजुट होकर मुख्यधारा की राजनीति में
हस्तक्षेप करने का शानदार मौका है. देश नए विकल्पों की ओर उम्मीद से देख रहा है.
('समकालीन जनमत' के मार्च'१२ अंक में प्रकाशित लेख)














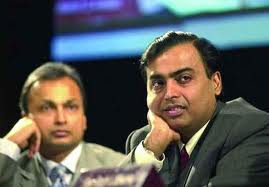







.jpg)



