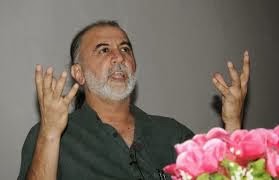लेकिन ख़बरों के इर्द-गिर्द है आयरन कर्टेन और लुटियन पत्रकारिता मुश्किल में
ऐसा लगता है कि सत्ता में बदलाव के साथ न सिर्फ सूचनाओं के स्रोत बदल गए हैं बल्कि खुद भाजपा और मोदी सरकार के अंदर सूचनाओं खासकर नकारात्मक सूचनाओं के बाहर आने पर पर सख्त नियंत्रण का युग शुरू हो चुका है.
 इस लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का वितरण सूचनाओं के
नियंत्रण और प्रबंधन के लिए खड़े किये जा रहे इस नए ‘लौह दीवार’ (आयरन कर्टेन) की
पहली परीक्षा थी जिसमें वह न सिर्फ कामयाब रही बल्कि उसने लुटियन दिल्ली के उन
धाकड़ पत्रकारों को ‘अटकलकारिता’ करने पर मजबूर कर दिया जो कल तक मंत्रिमंडल बनवाने
के दावे किया करते थे.
इस लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का वितरण सूचनाओं के
नियंत्रण और प्रबंधन के लिए खड़े किये जा रहे इस नए ‘लौह दीवार’ (आयरन कर्टेन) की
पहली परीक्षा थी जिसमें वह न सिर्फ कामयाब रही बल्कि उसने लुटियन दिल्ली के उन
धाकड़ पत्रकारों को ‘अटकलकारिता’ करने पर मजबूर कर दिया जो कल तक मंत्रिमंडल बनवाने
के दावे किया करते थे.
लेकिन यह सिर्फ चैनलों और अखबारों और मोदी सरकार के बीच शुरूआती हनीमून का नतीजा भर नहीं है बल्कि सूचनाओं खासकर नकारात्मक सूचनाओं/ख़बरों के बाहर निकलने पर आयद आयरन कर्टेन और सूचनाओं के अनुकूल प्रबंधन की सुविचारित रणनीति का भी नतीजा है.
मजे की बात यह है कि चैनल बिना किसी जांच-पड़ताल और छानबीन के उसे लपककर अपनी अटकलकारिता और फील गुड पत्रकारिता से खुश हैं. सचमुच, अच्छे दिन आ गए हैं.
दिल्ली में मोदी सरकार आने के साथ न्यूज मीडिया खासकर चैनलों की
‘पत्रकारिता’ में कई बदलाव दिखने लगे हैं. इसका पहला सुबूत यह है कि राजधानी के
धाकड़ रिपोर्टरों, सत्ता के गलियारों में दूर तक पहुंच रखनेवाले संवाददाताओं और
सर्वज्ञानी संपादकों को मोदी मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों और उनके विभागों के
बारे में तथ्यपूर्ण सूचनाएं नहीं थीं.
इसकी भरपाई वे परस्पर विरोधी सूचनाओं और
अटकलों से करने की कोशिश कर रहे थे. यहाँ तक कि ‘अच्छे दिन लौटने’ की उम्मीद कर
रहे भाजपा बीट के रिपोर्टरों के पास भी अटकलों के अलावा कुछ नहीं था.
नतीजा यह कि चैनल-दर-चैनल और अख़बारों तक में सिर्फ अटकलें थीं. चैनलों
पर घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक एंकरों, रिपोर्टरों और चर्चाकारों में संभावित
मंत्रिमंडल और मंत्रियों के विभागों को लेकर जिस तरह की अटकलबाजी चलती रही, क्या वह
न्यूज मीडिया में पत्रकारिता की बजाय ‘अटकलकारिता’ युग के आगमन का संकेत है? ऐसा लगता है कि सत्ता में बदलाव के साथ न सिर्फ सूचनाओं के स्रोत बदल गए हैं बल्कि खुद भाजपा और मोदी सरकार के अंदर सूचनाओं खासकर नकारात्मक सूचनाओं के बाहर आने पर पर सख्त नियंत्रण का युग शुरू हो चुका है.
 इस लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का वितरण सूचनाओं के
नियंत्रण और प्रबंधन के लिए खड़े किये जा रहे इस नए ‘लौह दीवार’ (आयरन कर्टेन) की
पहली परीक्षा थी जिसमें वह न सिर्फ कामयाब रही बल्कि उसने लुटियन दिल्ली के उन
धाकड़ पत्रकारों को ‘अटकलकारिता’ करने पर मजबूर कर दिया जो कल तक मंत्रिमंडल बनवाने
के दावे किया करते थे.
इस लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का वितरण सूचनाओं के
नियंत्रण और प्रबंधन के लिए खड़े किये जा रहे इस नए ‘लौह दीवार’ (आयरन कर्टेन) की
पहली परीक्षा थी जिसमें वह न सिर्फ कामयाब रही बल्कि उसने लुटियन दिल्ली के उन
धाकड़ पत्रकारों को ‘अटकलकारिता’ करने पर मजबूर कर दिया जो कल तक मंत्रिमंडल बनवाने
के दावे किया करते थे.
यह उन धाकड़ पत्रकारों/संपादकों के लिए एक चुनौती है जिनकी
‘पत्रकारिता’ लुटियन दिल्ली के भवनों और बंगलों की गणेश परिक्रमा में फल-फूल रही
थी. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे इस नए ‘आयरन कर्टेन’ से कैसे निपटें?
अफसोस यह कि इसका नतीजा सिर्फ अटकलकारिता में ही नहीं बल्कि ‘फील गुड
पत्रकारिता’ के पुनरागमन में भी दिख रहा है. आश्चर्य नहीं कि इन दिनों चैनलों और
अखबारों में नई सरकार के बारे में या तो गुडी-गुडी ‘खबरें’ चल रही हैं या उसे बिन
मांगी सलाहें दी जा रही हैं या फिर सरकार के लिए कारपोरेट समर्थित एजेंडा तय किया
जा रहा है. लेकिन यह सिर्फ चैनलों और अखबारों और मोदी सरकार के बीच शुरूआती हनीमून का नतीजा भर नहीं है बल्कि सूचनाओं खासकर नकारात्मक सूचनाओं/ख़बरों के बाहर निकलने पर आयद आयरन कर्टेन और सूचनाओं के अनुकूल प्रबंधन की सुविचारित रणनीति का भी नतीजा है.
यह नए प्रधानमंत्री की कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा रहा है. आश्चर्य
नहीं कि यह सरकार जहाँ एक ओर महत्वपूर्ण खासकर नकारात्मक सूचनाओं को नियंत्रित
करने की कोशिश कर रही है, वहीँ दूसरी ओर मीडिया को उदारतापूर्वक ‘खबरें’ और ‘विजुअल्स’
दी जा रही हैं.
ये वे फीलगुड ‘खबरें’ और ‘विजुअल्स’ हैं जिनमें वास्तविक और जनहित
से जुड़ी जानकारी कम और पी.आर ज्यादा है.
असल में, सरकार के मीडिया मैनेजरों को
अच्छी तरह से मालूम है कि 24X7
न्यूज चैनलों के दौर में चैनलों के पर्दे को भरना
और उन्हें चर्चा के लिए विषय देना बहुत जरूरी है.
इसलिए सूचना के प्रवाह को रोकने के बजाय उसे नियंत्रित और प्रबंधित
करने पर ज्यादा जोर है. आश्चर्य नहीं कि चैनलों के कैमरों को प्रधानमंत्री
कार्यालय से लेकर मंत्रिमंडल की बैठकों तक पहुँच दी गई है और आधिकारिक तौर पर हर
दिन चर्चा के लिए अनुकूल विषय भी दिए जा रहे हैं. मजे की बात यह है कि चैनल बिना किसी जांच-पड़ताल और छानबीन के उसे लपककर अपनी अटकलकारिता और फील गुड पत्रकारिता से खुश हैं. सचमुच, अच्छे दिन आ गए हैं.
('तहलका' के 15 जून के अंक में प्रकाशित टिप्पणी का असंपादित अंश)



.jpg)