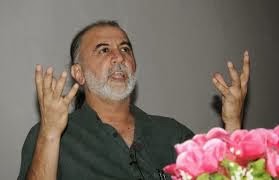राष्ट्रीय मीडिया उत्तर पूर्व को एक खास “राष्ट्रवादी” वैचारिक खांचे में देखता है
ऐसा लग रहा था कि जैसे बहाने बना रहा हूँ और जिसका बचाव नहीं किया जा सकता है, उसका असफल बचाव करने की कोशिश कर रहा हूँ. सच यही है कि उत्तर-पूर्व दिल्ली के राष्ट्रीय न्यूज मीडिया में एक बारीक और कई बार बहुत नग्न और बर्बर किस्म की नस्लीय उपेक्षा और पूर्वाग्रहों का शिकार है.
बात वहीँ खत्म नहीं हुई. उसके बाद से लगातार सोचता रहा कि आखिर हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनलों से उत्तर-पूर्व क्यों गायब है? क्या वह देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां की राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक घटनाओं के बारे में देश के बाकी हिस्सों के लोगों को नहीं जानना चाहिए? वहां के लोग देश के बाकी हिस्सों से किसी मायने में कमतर हैं?
 खुद उत्तर पूर्व के लोग राष्ट्रीय चैनलों में अपने इलाके और समाज को न
देखकर क्या महसूस करते होंगे? बात-बात पर राष्ट्रभक्ति का राग अलापनेवाले चैनलों
के लिए आखिर उत्तर-पूर्व के क्या मायने हैं और वह उनके न्यूज एजेंडा में कहाँ है?
खुद उत्तर पूर्व के लोग राष्ट्रीय चैनलों में अपने इलाके और समाज को न
देखकर क्या महसूस करते होंगे? बात-बात पर राष्ट्रभक्ति का राग अलापनेवाले चैनलों
के लिए आखिर उत्तर-पूर्व के क्या मायने हैं और वह उनके न्यूज एजेंडा में कहाँ है?
तथ्य यह है कि जब कभी उत्तर-पूर्व चैनलों पर दिखता भी है तो वह किसी बड़े एथनिक नरसंहार या बम विस्फोट में बड़ी संख्या में मारे जाने या कन्फ्लिक्ट की किसी ऐसी बड़ी घटना के कारण दिखता है या फिर चीन की कथित घुसपैठ या अरुणाचल पर चीन के दावे या विभिन्न अलगाववादी आन्दोलनों और उनकी हिंसक कार्रवाइयों के कारण गाहे-बगाहे सुर्ख़ियों में दिख जाता है.
गोया उत्तर-पूर्व में एथनिक झगडों, अलगाववादी आन्दोलनों, तनावों, हत्याओं, नरसंहारों के अलावा और कुछ होता ही नहीं है. कहने की जरूरत नहीं है कि इससे राष्ट्रीय मीडिया में उत्तर पूर्व की एक इकहरी छवि बन गई है जो नस्ली भेदभाव का ही विस्तार और उसे मजबूत करने में मदद करती है.
इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले और प्रदर्शनकारियों के दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्रियों और नेताओं से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ने नस्ली भेदभाव के मुद्दे को न सिर्फ जिन्दा रखा बल्कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई और न्यूज मीडिया को कवरेज देने के लिए मजबूर किया.
 असल में, दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व के लोगों
के साथ नस्ली भेदभाव का मुद्दा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे जानबूझकर अनदेखा
किया जाता है या छुपाया-दबाया जाता है. यही नहीं, मीडिया और राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग
के एक ‘राष्ट्रवादी’ हिस्से को लगता है कि उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली
भेदभाव और छींटाकशी की सच्चाई को स्वीकार करने पर इसका फायदा उत्तर पूर्व के
अलगाववादी समूह उठाएंगे.
असल में, दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व के लोगों
के साथ नस्ली भेदभाव का मुद्दा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे जानबूझकर अनदेखा
किया जाता है या छुपाया-दबाया जाता है. यही नहीं, मीडिया और राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग
के एक ‘राष्ट्रवादी’ हिस्से को लगता है कि उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली
भेदभाव और छींटाकशी की सच्चाई को स्वीकार करने पर इसका फायदा उत्तर पूर्व के
अलगाववादी समूह उठाएंगे.
इसलिए वह सच्चाई से अवगत होते हुए भी न सिर्फ उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से हिचकिचाता है बल्कि अक्सर उसे सख्ती से नकारने की कोशिश करता है. इसी तरह मीडिया और राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग के एक हिस्से को लगता है कि यह भेदभाव सिर्फ उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नहीं बल्कि दिल्ली में दक्षिण और मुंबई में बिहार-यू.पी आदि के लोगों के साथ भी होता है. इसी तर्क के आधार पर कुछ साल पहले तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव के आरोपों को नकारने की कोशिश की थी.
इसके अलावा नार्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर और हेल्पलाइन की २००९ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्व के ८६ फीसदी से ज्यादा लोगों को नस्ली भेदभाव और यौन उत्पीडन (सेक्सुअल हैरेसमेंट) का शिकार होना पड़ता है. इन रिपोर्टों से साफ़ है कि उत्तर पूर्व के लोगों को अपने ही देश और उसकी राजधानी में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है.
 अच्छी बात यह है कि न्यूज मीडिया और चैनलों के बड़े हिस्से ने इसे
नस्ली भेदभाव के एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए मुद्दा बनाया. असल में, देश की
राजधानी में उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होनेवाला नस्ली भेदभाव एक ऐसा बर्बर और
कड़वा सच है जिसे जानते सब हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के लिए कम ही
तैयार होते हैं.
अच्छी बात यह है कि न्यूज मीडिया और चैनलों के बड़े हिस्से ने इसे
नस्ली भेदभाव के एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए मुद्दा बनाया. असल में, देश की
राजधानी में उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होनेवाला नस्ली भेदभाव एक ऐसा बर्बर और
कड़वा सच है जिसे जानते सब हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के लिए कम ही
तैयार होते हैं.
चाहे पुलिस-प्रशासन हो या मीडिया या फिर सिविल सोसायटी- सब अलग-अलग कारणों से उससे आँख चुराते हैं या बहुत दबी जुबान में चर्चा करते हैं. उन्हें इससे ‘देश की छवि’ से लेकर ‘उत्तर पूर्व में अलगाववादियों द्वारा भुनाने’ की चिंता सताने लगती है. लेकिन इससे समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है.
हालाँकि इस फैसले पर हंगामे के बाद मुनिरका के स्थानीय मकान-मालिकों ने उत्तर पूर्व के लोगों के बारे में ऐसा कोई फैसला करने से इनकार करते दावा किया कि वे सिर्फ ‘नशा करने, हंगामा करने और रात को देर से घर लौटनेवालों’ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि उनके निशाने पर कौन है और क्यों?
यही नहीं, जब चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्व के कई युवाओं को तिब्बती समझकर पकड़ लिया और थाने में बैठाए रहे. मामला सिर्फ दिल्लीवालों, दिल्ली पुलिस और प्रशासन तक सीमित नहीं है बल्कि सच यह है कि इस नस्ली भेदभाव की जड़ें काफी गहरी और व्यापक हैं और आम जनजीवन का कोई भी वर्ग और समूह इसके प्रभाव से बचा हुआ नहीं है.
 मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है. राष्ट्रीय मीडिया खासकर न्यूज चैनल
उत्तर पूर्व को एक खास “राष्ट्रवादी” वैचारिक खांचे में देखते हैं और उत्तर पूर्व
के बारे में अपनी कवरेज में प्रचलित पूर्वाग्रहों और स्टीरियोटाइप्स को ही मजबूत
करते हैं.
मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है. राष्ट्रीय मीडिया खासकर न्यूज चैनल
उत्तर पूर्व को एक खास “राष्ट्रवादी” वैचारिक खांचे में देखते हैं और उत्तर पूर्व
के बारे में अपनी कवरेज में प्रचलित पूर्वाग्रहों और स्टीरियोटाइप्स को ही मजबूत
करते हैं.
लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्थिति बदलेगी या फिर कुछ दिनों बाद फिर किसी नीडो को जान देनी पड़ेगी? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर पूर्व के लोगों के साथ लंबे समय से जारी नस्ली भेदभाव के लिए एक खास सवर्ण हिंदू राष्ट्रवादी-मर्दवादी-नस्लवादी मानसिकता जिम्मेदार है जिसकी जड़ें पुलिस-प्रशासन से लेकर मीडिया तक में फैली हुईं है.
इसके शिकार सिर्फ उत्तर पूर्व के ही नहीं बल्कि सभी कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम-सिख और आदिवासी आदि हैं.
यह एक तथ्य है कि अधिकांश राष्ट्रीय चैनलों खासकर हिंदी न्यूज चैनलों के न्यूजरूम में उत्तर पूर्व के लोगों की संख्या नगण्य है, वे फैसले लेने की जगहों पर नहीं हैं और उत्तर पूर्व के राज्यों में उनके संवाददाता भी नहीं हैं.
यही नहीं, इन चैनलों के रिपोर्टर/संपादक शायद ही कभी उत्तर पूर्व के राज्यों की रिपोर्टिंग पर गए हों. आश्चर्य नहीं कि न्यूजरूम में ऐसे गेटकीपरों और रिपोर्टरों की संख्या बहुतायत में है जो कभी उत्तर पूर्व नहीं गए और वहां के बारे में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर धारणाएं बना रखी हैं.
अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की दिल्ली के पाश बाजार लाजपतनगर
में नस्लीय हत्या और उसकी न्यूज मीडिया में कवरेज ने पिछले साल अक्टूबर में कोई
पन्द्रह दिनों के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की यात्रा की दिला दी.
ईटानगर के पास रानो हिल्स स्थित राजीव गाँधी विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं को
पत्रकारिता पढ़ाने गया था.
वहीँ मीडिया खासकर न्यूज चैनलों पर चर्चा के दौरान एक
छात्रा ने पूछा, ‘देश के बड़े और राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर उत्तर-पूर्व के राज्य
और उनकी खबरें क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं?’ प्रश्न बहुत सीधा था और शायद उत्तर भी
कि उत्तर-पूर्व नस्लीय भेदभाव का शिकार है.
हालाँकि उत्तर-पूर्व की रुटीन घटनाओं में राष्ट्रीय खबर बनने लायक
न्यूज वैल्यू न होने से लेकर दिल्ली से दूरी जैसे तर्कों के जरिये विद्यार्थियों
के सामने न्यूज चैनलों का पक्ष रखने की भी कोशिश की और खूब गरमागरम बहस भी हुई लेकिन
सच यह है कि खुद इन कमजोर तर्कों से सहमत नहीं था. ऐसा लग रहा था कि जैसे बहाने बना रहा हूँ और जिसका बचाव नहीं किया जा सकता है, उसका असफल बचाव करने की कोशिश कर रहा हूँ. सच यही है कि उत्तर-पूर्व दिल्ली के राष्ट्रीय न्यूज मीडिया में एक बारीक और कई बार बहुत नग्न और बर्बर किस्म की नस्लीय उपेक्षा और पूर्वाग्रहों का शिकार है.
बात वहीँ खत्म नहीं हुई. उसके बाद से लगातार सोचता रहा कि आखिर हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनलों से उत्तर-पूर्व क्यों गायब है? क्या वह देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां की राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक घटनाओं के बारे में देश के बाकी हिस्सों के लोगों को नहीं जानना चाहिए? वहां के लोग देश के बाकी हिस्सों से किसी मायने में कमतर हैं?
 खुद उत्तर पूर्व के लोग राष्ट्रीय चैनलों में अपने इलाके और समाज को न
देखकर क्या महसूस करते होंगे? बात-बात पर राष्ट्रभक्ति का राग अलापनेवाले चैनलों
के लिए आखिर उत्तर-पूर्व के क्या मायने हैं और वह उनके न्यूज एजेंडा में कहाँ है?
खुद उत्तर पूर्व के लोग राष्ट्रीय चैनलों में अपने इलाके और समाज को न
देखकर क्या महसूस करते होंगे? बात-बात पर राष्ट्रभक्ति का राग अलापनेवाले चैनलों
के लिए आखिर उत्तर-पूर्व के क्या मायने हैं और वह उनके न्यूज एजेंडा में कहाँ है? तथ्य यह है कि जब कभी उत्तर-पूर्व चैनलों पर दिखता भी है तो वह किसी बड़े एथनिक नरसंहार या बम विस्फोट में बड़ी संख्या में मारे जाने या कन्फ्लिक्ट की किसी ऐसी बड़ी घटना के कारण दिखता है या फिर चीन की कथित घुसपैठ या अरुणाचल पर चीन के दावे या विभिन्न अलगाववादी आन्दोलनों और उनकी हिंसक कार्रवाइयों के कारण गाहे-बगाहे सुर्ख़ियों में दिख जाता है.
गोया उत्तर-पूर्व में एथनिक झगडों, अलगाववादी आन्दोलनों, तनावों, हत्याओं, नरसंहारों के अलावा और कुछ होता ही नहीं है. कहने की जरूरत नहीं है कि इससे राष्ट्रीय मीडिया में उत्तर पूर्व की एक इकहरी छवि बन गई है जो नस्ली भेदभाव का ही विस्तार और उसे मजबूत करने में मदद करती है.
इस अर्थ में दिल्ली में नीडो तानिया की नस्ली हत्या के लिए जमीन तैयार
करने में न्यूज मीडिया की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. यह सच है कि
नीडो की हत्या के मुद्दे को राष्ट्रीय न्यूज मीडिया में काफी जगह मिली. न्यूज
मीडिया के एक बड़े हिस्से ने उत्तर पूर्व के लोगों के साथ राजधानी में नस्लीय
भेदभाव को मुद्दा बनाया.
इससे सरकार, पुलिस-प्रशासन और राजनीतिक दलों पर दिल्ली और
देश के दूसरे शहरों में नस्लीय भेदभाव, छींटाकशी और हमलों के शिकार उत्तर पूर्व के
लोगों खासकर विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों को संरक्षण देने और दोषियों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा.
लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि नीडो तानिया की हत्या के मुद्दे को न्यूज
मीडिया से पहले दिल्ली में रहनेवाले उत्तर पूर्व के युवाओं और सजग नागरिक समाज के
एक हिस्से ने जोरशोर से उठाया. उनकी सक्रियता और लाजपतनगर थाने पर जोरदार प्रदर्शन
के कारण न्यूज मीडिया खासकर चैनलों पर भी इसके कवरेज का दबाव बढ़ा. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले और प्रदर्शनकारियों के दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्रियों और नेताओं से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ने नस्ली भेदभाव के मुद्दे को न सिर्फ जिन्दा रखा बल्कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई और न्यूज मीडिया को कवरेज देने के लिए मजबूर किया.
अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर उत्तर पूर्व के युवाओं और दिल्ली
के नागरिक समाज खासकर जे.एन.यू छात्रसंघ और आइसा सहित दूसरे वाम-जनवादी छात्र
संगठनों ने राजधानी की सड़कों पर लगातार इस मुद्दे को उठाया नहीं होता और उत्तर
पूर्व के लोगों के साथ वर्षों से जारी नस्ली भेदभाव, छींटाकशी और हमलों को मुद्दा
नहीं बनाया होता तो क्या न्यूज मीडिया और चैनल इस मुद्दे को इतना कवरेज देते या
नस्ली भेदभाव को मुद्दा बनाते?
अनुभव यही बताता है कि राष्ट्रीय मीडिया के लिए
राजधानी और देश के बाकी हिस्सों में उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव कोई
मुद्दा नहीं रहा है. अगर रहा होता तो शायद नीडो की जान नहीं जाती.
 असल में, दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व के लोगों
के साथ नस्ली भेदभाव का मुद्दा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे जानबूझकर अनदेखा
किया जाता है या छुपाया-दबाया जाता है. यही नहीं, मीडिया और राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग
के एक ‘राष्ट्रवादी’ हिस्से को लगता है कि उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली
भेदभाव और छींटाकशी की सच्चाई को स्वीकार करने पर इसका फायदा उत्तर पूर्व के
अलगाववादी समूह उठाएंगे.
असल में, दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व के लोगों
के साथ नस्ली भेदभाव का मुद्दा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे जानबूझकर अनदेखा
किया जाता है या छुपाया-दबाया जाता है. यही नहीं, मीडिया और राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग
के एक ‘राष्ट्रवादी’ हिस्से को लगता है कि उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली
भेदभाव और छींटाकशी की सच्चाई को स्वीकार करने पर इसका फायदा उत्तर पूर्व के
अलगाववादी समूह उठाएंगे. इसलिए वह सच्चाई से अवगत होते हुए भी न सिर्फ उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से हिचकिचाता है बल्कि अक्सर उसे सख्ती से नकारने की कोशिश करता है. इसी तरह मीडिया और राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग के एक हिस्से को लगता है कि यह भेदभाव सिर्फ उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नहीं बल्कि दिल्ली में दक्षिण और मुंबई में बिहार-यू.पी आदि के लोगों के साथ भी होता है. इसी तर्क के आधार पर कुछ साल पहले तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने उत्तर पूर्व के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव के आरोपों को नकारने की कोशिश की थी.
लेकिन नीडो तानिया की हत्या के बाद राजधानी में जिस बड़ी संख्या में
उत्तर पूर्व के युवा सड़कों पर उतर आए और अपने गुस्से और पीड़ा का इजहार किया, उससे
साफ़ है कि यह मामला सामान्य झगडे-मारपीट और हत्या का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा
गंभीर है. अगर यह एक सामान्य हत्या की घटना होती तो उत्तर पूर्व के हजारों युवा
सड़कों पर नहीं उतर आते.
सच यह है कि नीडो तानिया की मौत एक ट्रिगर की तरह थी जिससे
रोजमर्रा के जीवन में नस्ली भेदभाव, छींटाकशी और हमलों को झेलनेवाले उत्तर पूर्व
को लोगों के दबे गुस्से और पीड़ा को फूटकर बाहर आने का मौका दिया.
कई स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्ट्स इस कड़वी सच्चाई की पुष्टि करती है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फार नार्थ ईस्ट एंड पॉलिसी रिसर्च की एक
सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहनेवाले उत्तर
पूर्व के ८१ प्रतिशत नागरिकों ने स्वीकार किया कि उन्हें कालेज, विश्वविद्यालय,
बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नस्लीय भेदभाव और छींटाकशी का शिकार होना पड़ता
है. इसके अलावा नार्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर और हेल्पलाइन की २००९ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्व के ८६ फीसदी से ज्यादा लोगों को नस्ली भेदभाव और यौन उत्पीडन (सेक्सुअल हैरेसमेंट) का शिकार होना पड़ता है. इन रिपोर्टों से साफ़ है कि उत्तर पूर्व के लोगों को अपने ही देश और उसकी राजधानी में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है.
इसके बावजूद न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों का एक हिस्सा इसबार भी
नीडो तानिया की हत्या को नस्ली भेदभाव का मामला मानने से इनकार करते हुए इसे
तात्कालिक उत्तेजना में हुए झगडे और मारपीट के मामले की तरह पेश करता रहा.
सबसे अफ़सोस
की बात यह है कि शुरू में कई चैनलों और उनके रिपोर्टरों ने पुलिस के तोते की तरह
नीडो की मौत को ‘मामूली मारपीट’ और ‘ड्रग्स के ओवरडोज’ जैसी स्टीरियोटाइप
‘स्टोरीज’ से दबाना-छुपाना चाहा.
लेकिन सलाम करना चाहिए उत्तर पूर्व के उन सैकड़ों
छात्र-युवाओं और प्रगतिशील-रैडिकल छात्र संगठनों का जिन्होंने नीडो की नस्ली हत्या
के बाद लाजपतनगर से लेकर जंतर-मंतर तक अपने गुस्से और विरोध का इतना जुझारू इजहार
किया कि मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों-नेताओं और सरकार-पुलिस-प्रशासन को उसे अनदेखा
करना मुश्किल हो गया.
 अच्छी बात यह है कि न्यूज मीडिया और चैनलों के बड़े हिस्से ने इसे
नस्ली भेदभाव के एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए मुद्दा बनाया. असल में, देश की
राजधानी में उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होनेवाला नस्ली भेदभाव एक ऐसा बर्बर और
कड़वा सच है जिसे जानते सब हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के लिए कम ही
तैयार होते हैं.
अच्छी बात यह है कि न्यूज मीडिया और चैनलों के बड़े हिस्से ने इसे
नस्ली भेदभाव के एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए मुद्दा बनाया. असल में, देश की
राजधानी में उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होनेवाला नस्ली भेदभाव एक ऐसा बर्बर और
कड़वा सच है जिसे जानते सब हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के लिए कम ही
तैयार होते हैं. चाहे पुलिस-प्रशासन हो या मीडिया या फिर सिविल सोसायटी- सब अलग-अलग कारणों से उससे आँख चुराते हैं या बहुत दबी जुबान में चर्चा करते हैं. उन्हें इससे ‘देश की छवि’ से लेकर ‘उत्तर पूर्व में अलगाववादियों द्वारा भुनाने’ की चिंता सताने लगती है. लेकिन इससे समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है.
विडम्बना देखिए कि दिल्ली और देश के अन्य राज्यों/शहरों में उत्तर
पूर्व के लोगों को जिस तरह का नस्ली भेदभाव, उत्पीडन और अपमान झेलना पड़ता है, उसे
मुद्दा बनाने और न्यूज मीडिया सहित नागरिक समाज की चेतना को झकझोरने के लिए
अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया को अपनी जान देनी पड़ी.
हालाँकि नीडो नस्ली
भेदभाव की कीमत चुकानेवाला पहला युवा नहीं है और स्थितियां नहीं बदलीं तो वह आखिरी
भी नहीं है. हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि
नीडो की हत्या का खून अभी सूखा भी नहीं था कि राजधानी के मुनिरका में मणिपुर की एक
बच्ची के साथ बलात्कार और साकेत में एक युवा पर जानलेवा हमले का मामला सामने आ
गया.
जैसे इतना ही काफी नहीं हो, इस घटना के बाद मुनिरका गांव की रेजिडेंट
वेलफेयर एसोशियेसन ने बिलकुल खाप की तरह व्यवहार करते हुए उत्तर पूर्व के लोगों पर
कई तरह की बेतुकी पाबंदियां आयद कर दीं. यही नहीं, मुनिरका के मकान-मालिकों ने
उत्तर पूर्व के लोगों घरों से निकालने और उन्हें घर न देने का फैसला भी कर लिया. हालाँकि इस फैसले पर हंगामे के बाद मुनिरका के स्थानीय मकान-मालिकों ने उत्तर पूर्व के लोगों के बारे में ऐसा कोई फैसला करने से इनकार करते दावा किया कि वे सिर्फ ‘नशा करने, हंगामा करने और रात को देर से घर लौटनेवालों’ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि उनके निशाने पर कौन है और क्यों?
हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन
मकान-मालिकों के फैसले के आगे अपनी विवशता भी जाहिर कर दी क्योंकि यह उनका
‘अधिकार’ है कि वे किसे किरायेदार रखें और किसे नहीं? सवाल यह है कि क्या यह नस्ली
भेदभाव का एक और सुबूत नहीं है?
ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती
थीं लेकिन होता यह था कि या तो उन्हें दबा दिया जाता दिया जाता था या फिर उन्हें
रुटीन अपराध के मामले मानकर निपटा दिया जाता था. नस्ली छींटाकशी और उपहास तो जैसे
आम बात है. उत्तर पूर्व के लोगों के रहन-सहन और खान-पान से लेकर बात-व्यवहार के
बारे में आम दिल्लीवालों में अनेकों भ्रामक धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स और पूर्वाग्रह
हैं.
यहाँ तक कि खुद पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी का रवैय्या भी कम भेदभावपूर्ण
नस्ली नहीं है. विभिन्न मामलों में दिल्ली पुलिस का व्यवहार भी उसी पूर्वाग्रह और
स्टीरियोटाइप्स से संचालित होता रहा है. उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस ने उत्तर
पूर्व के लोगों के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के बजाय उल्टे उत्तर
पूर्व के लोगों के लिए दिल्ली में “क्या करें और क्या न करें” की लंबी सूची जारी
की हुई है. यही नहीं, जब चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्व के कई युवाओं को तिब्बती समझकर पकड़ लिया और थाने में बैठाए रहे. मामला सिर्फ दिल्लीवालों, दिल्ली पुलिस और प्रशासन तक सीमित नहीं है बल्कि सच यह है कि इस नस्ली भेदभाव की जड़ें काफी गहरी और व्यापक हैं और आम जनजीवन का कोई भी वर्ग और समूह इसके प्रभाव से बचा हुआ नहीं है.
 मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है. राष्ट्रीय मीडिया खासकर न्यूज चैनल
उत्तर पूर्व को एक खास “राष्ट्रवादी” वैचारिक खांचे में देखते हैं और उत्तर पूर्व
के बारे में अपनी कवरेज में प्रचलित पूर्वाग्रहों और स्टीरियोटाइप्स को ही मजबूत
करते हैं.
मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है. राष्ट्रीय मीडिया खासकर न्यूज चैनल
उत्तर पूर्व को एक खास “राष्ट्रवादी” वैचारिक खांचे में देखते हैं और उत्तर पूर्व
के बारे में अपनी कवरेज में प्रचलित पूर्वाग्रहों और स्टीरियोटाइप्स को ही मजबूत
करते हैं.
उदाहरण के लिए, अन्ना हजारे के अनशन को 24X7 कवरेज
देनेवाले और उन्हें ‘महानायक’ बनानेवाले चैनलों ने मणिपुर में सशस्त्र सैन्यबल
विशेषाधिकार कानून के खिलाफ पिछले १४ साल से अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला की कितनी
बार सुध ली?
यह सिर्फ एक उदाहरण है लेकिन उत्तर पूर्व में ऐसे अनेकों
मामले/मुद्दे/घटनाएँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय मीडिया ने या तो अनदेखा किया या फिर
तोडमरोड कर पेश किया है.
लेकिन नीडो की मौत के बाद लगता है उत्तर-पूर्व के युवाओं का धैर्य
जवाब देने लगा है. वे इसे और सहने के बजाय इससे लड़ने और चुनौती देने का मन बना
चुके हैं. अच्छी बात यह है कि इससे चैनलों-अख़बारों से लेकर सिविल सोसायटी की
अंतरात्मा भी जागी दिखती है. अगले कुछ महीनों में होनेवाले लोकसभा चुनावों के कारण
नेताओं का दिल भी उत्तर पूर्व के लोगों के लिए फटा जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्थिति बदलेगी या फिर कुछ दिनों बाद फिर किसी नीडो को जान देनी पड़ेगी? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर पूर्व के लोगों के साथ लंबे समय से जारी नस्ली भेदभाव के लिए एक खास सवर्ण हिंदू राष्ट्रवादी-मर्दवादी-नस्लवादी मानसिकता जिम्मेदार है जिसकी जड़ें पुलिस-प्रशासन से लेकर मीडिया तक में फैली हुईं है.
इसके शिकार सिर्फ उत्तर पूर्व के ही नहीं बल्कि सभी कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम-सिख और आदिवासी आदि हैं.
यह इतनी आसानी से खत्म होनेवाला नहीं है. इससे लड़ने के लिए न सिर्फ इस
मानसिकता को चुनौती देने और एक सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है बल्कि
नस्लभेद के उन सभी दबे-छिपे रूपों और स्टीरियोटाइप्स को खुलकर नकारना और सार्वजनिक
स्थानों/मंचों को नस्ली रूप से ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाना होगा.
अपने न्यूज
चैनलों को ही देख लीजिए, उनके कितने एंकर/रिपोर्टर उत्तर पूर्व के हैं? इन चैनलों
पर उत्तर पूर्व की ख़बरों को कितनी जगह मिलती है? कितने चैनलों के उत्तर पूर्व में
रिपोर्टर हैं? यही नहीं, मनोरंजन चैनलों पर कितने धारावाहिकों के पात्र या कथानक उत्तर
पूर्व के हैं?
मनोरंजन से लेकर न्यूज चैनलों तक में उत्तर पूर्व के लोगों और इलाके
के प्रतिनिधित्व और उनकी पूर्वाग्रहों से मुक्त प्रस्तुति का सवाल बहुत महत्वपूर्ण
है क्योंकि लोगों को शिक्षित करने और उनमें संवेदनशीलता पैदा करने में मीडिया की
भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. यह एक तथ्य है कि अधिकांश राष्ट्रीय चैनलों खासकर हिंदी न्यूज चैनलों के न्यूजरूम में उत्तर पूर्व के लोगों की संख्या नगण्य है, वे फैसले लेने की जगहों पर नहीं हैं और उत्तर पूर्व के राज्यों में उनके संवाददाता भी नहीं हैं.
यही नहीं, इन चैनलों के रिपोर्टर/संपादक शायद ही कभी उत्तर पूर्व के राज्यों की रिपोर्टिंग पर गए हों. आश्चर्य नहीं कि न्यूजरूम में ऐसे गेटकीपरों और रिपोर्टरों की संख्या बहुतायत में है जो कभी उत्तर पूर्व नहीं गए और वहां के बारे में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर धारणाएं बना रखी हैं.
क्या नीडो की मौत के बाद न्यूज मीडिया अपने अंदर भी झांकेगा? क्या इस
‘पब्लिक स्फीयर’ में भी हम कुछ बदलाव की उम्मीद करें?
('कथादेश' के मार्च'2014 अंक में प्रकाशित स्तम्भ)